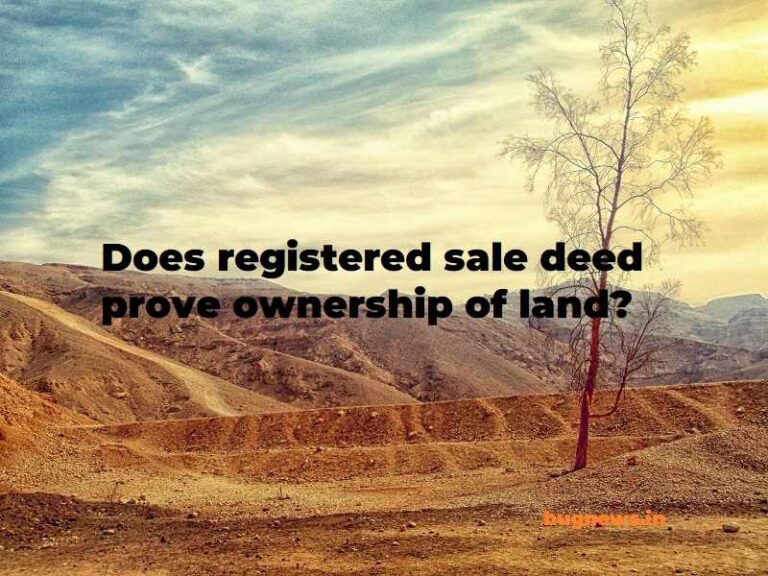बौद्ध मूर्तिकला की एक अनूठी शैली जिसे गांधार कला कहा जाता है, प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के गांधार क्षेत्र में विकसित हुई, जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। यह क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान में भी विस्तारित हुआ। गांधार मूर्तिकला शैली का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। गांधार मूर्तिकला शैली में विशिष्ट प्रकार की बुद्ध प्रतिमा विकसित की । शैली प्राचीन ग्रीस और रोम की कला से काफी प्रभावित थी, लेकिन यह काफी हद तक मूल रचना भारतीय परंपराओं से भी प्रभावित थी। गांधार मूर्तिकला इस प्रकार पश्चिमी और पूर्वी कला दोनों के मिश्रित तत्व हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जहां कहीं भी पुरातात्विक खुदाई की जाती है, वहां बौद्ध धर्म की उपस्थिति अधिक होती है, पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में खुदाई के दौरान गौतम बुद्ध की एक दुर्लभ आदमकद प्रतिमा मिली थी। खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत का यह क्षेत्र श्रीलंका, कोरिया और जापान के बौद्धों के लिए एक पर्यटन स्थल है, क्योंकि यह क्षेत्र उपमहाद्वीप के इतिहास में गांधार कला की शुरुआती शहरी बस्तियों में से एक है।
खैबर-पख्तूनख्वा का प्राचीन नाम गांधार है, यहां की खुदाई में प्राचीन काल में बनी कई गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमाएं अक्सर मिलती रहती है।
गांधार क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास
गांधार क्षेत्र प्राचीन भारत में लंबे समय तक सांस्कृतिक राजनीतिक और व्यापारिक रूप से इतिहास का एक चलायमान जगह रही है। वर्तमान में गांधार क्षेत्र को उत्तर पश्चिम कश्मीर, उत्तर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवस्थिति से पहचान सकते है। यह क्षेत्र प्रसिद्ध सिल्क रुट के कारण समृद्ध रहा था।
गांधार क्षेत्र 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी शासन के अधीन आया था और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इसे जीत लिया था। इसके बाद गांधार पर भारत के मौर्य वंश का शासन था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, गांधार बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र बन गया। पहली शताब्दी ईस्वी में, यह क्षेत्र कुषाण साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कुषाण साम्राज्य के शासकों ने रोम के साथ संपर्क बनाए रखा।
भारतीय सम्राट अशोक (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान, यह क्षेत्र गहन बौद्ध गतिविधियों का केंद्र बन गया था और पहली शताब्दी ईस्वी में, कुषाण साम्राज्य के शासकों सिल्क मार्ग से रोम के साथ संपर्क बनाए रखा। प्राचीन बौद्ध लेखन में, गांधार स्कूल ने शास्त्रीय रोमन कला से कई रूपांकनों और तकनीकों को शामिल किया, हालाँकि, मूल प्रतिमा भारतीय बनी रही।
गांधार शैली की स्थापना किसने की थी?
उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाणों के शासनकाल में मूर्तिकला की एक नई शैली विकसित हुई। यह भारतीय और यूनानी मूर्तिकला का मिश्रित रूप था। गांधार क्षेत्र के आधार पर जिसमें यह शैली विकसित हुई, इसे ‘गांधार मूर्तिकला‘ के रूप में जाना जाने लगा। कनिष्क और उनके उत्तराधिकारियों ने गांधार शैली को बढ़ावा दिया।
गांधार की मूर्तिकला पर ग्रीक मूर्तिकला का गहरा प्रभाव था जिसमें मानव प्रतिनिधित्व के बाहरी पहलू को अधिक महत्व दिया जाता है। गांधार मूर्तिकला का विषय भारतीय था, लेकिन मूर्तिकला की शैली ग्रीक और रोमन थी, इसलिए गांधार मूर्तिकला को ग्रीको-रोमन, ग्रीको-बौद्ध या हिंदू-ग्रीक मूर्तिकला भी कहा जाता है।
गांधार शैली के केंद्र
इसके मुख्य केंद्र जलालाबाद, हददा, बामियान, स्वात घाटी और पेशावर थे। इस मूर्ति में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं।
गांधार शैली कब विकसित हुई ?
गांधार शैली की मूर्तियां पहली शताब्दी ईस्वी से चौथी शताब्दी ईस्वी तक की हैं और इस शैली की सर्वश्रेष्ठ कृतियों को 50 ईस्वी से 150 ईस्वी तक माना जा सकता है।
गांधार शैली की विशेषताएं
इसके निर्माण में काले और सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। महायान धर्म के विकास ने गांधार की कला को बढ़ावा दिया। उनकी मूर्तियों की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और आकर्षक परिधान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस शैली के कारीगरों ने वास्तविकता पर थोड़ा ध्यान देकर बाहरी सुंदरता को मूर्त रूप देने की कोशिश की।

दाढ़ी वाली आकृति बाईं ओर घुटनों के बल जमीन पर बैठी है और हाथों को घुटनों पर रखा गया है; चिकनी-चेहरे वाली आकृति दाईं ओर जमीन पर बैठी है, दाहिना घुटना उठा हुआ है और कोहनी उस पर टिकी हुई है
उनकी मूर्तियों में, भगवान बुद्ध ग्रीक देवता अपोलो के समान प्रतीत होते हैं। इस शैली में सुन्दर नक्काशी का प्रयोग करते हुए प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि का सुन्दर संयोजन प्रस्तुत किया गया है। इस शैली में आभूषणों का अधिक प्रदर्शन किया गया है।
इसमें सिर के पिछले हिस्से पर बालों को मोड़कर बनाया गया एक बाल है, जिससे मूर्तियां बहुत अच्छी और जीवंत दिखती हैं। कनिष्क के समय में गांधार की कला का बहुत तेजी से विकास हुआ। भरहुत और सांची में कनिष्क द्वारा बनाए गए स्तूप गांधार की कला के उदाहरण हैं।

गहरे भूरे रंग के सूक्ष्म स्लेट पत्थर से बने सिर के पीछे सादे गोल प्रभामंडल के साथ खड़े बुद्ध। पैरों के नीचे की कुर्सी को दो खूबसूरत रस्सियों से सजाया गया है। उनके हाथ अभय और वर मुद्रा में थे लेकिन टूट गए हैं। दाहिने हाथ में एक डॉवेल छेद देखा जा सकता है। वस्त्र और सुडौल बाल गांधार बौद्ध मूर्तिकला की विशेषता है और ग्रीको-रोमन प्रभाव दिखाता है।
गांधार कला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं मुख्य विषय के रूप में जैसे इसमें जातक कथाये महत्वपूर्ण है जो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म को उकेरती है साथ साथ बोधिसत्व से सम्बंधित घटनाये शामिल है
- इंडो – यूनानी कला प्रभाव स्पष्ट है जैसे मूर्तियों में बुद्ध का चेहरा ग्रीक देवता अपोलो जैसा दिखता है और शरीर की बनावट यथार्थवादी है
- ग्रीक किंवदंतियों और देवी-देवताओं भी विद्यमान है
- मूर्तियां बनाने का तरीका विशुद्ध भारतीय है जैसे शरीर की बनावट, बुद्ध के चोगे पर पड़ी सलवटे , एक यूनानी पेड़ के बिच बैठे गौतम बुद्ध, यक्ष और कुबेर के दृश्य, शानदार नक्काशी आदि
- गांधार शैली में केवल बौद्ध धर्म से सम्बंधित मूर्तियाँ बनायीं गयी
गांधार कला पर ग्रीको-रोमन प्रभाव
- भगवान बुद्ध के सिर के पीछे प्रभामंडल
- बुद्ध के लहराते घुंघराले बाल
- सिर के ललाट पर रेखाएं
- गहने और आभूषण
- ड्रेप और कपड़ों की शैली
गांधार शैली में उपयोग में आने वाली रंग और तरीके
गांधार मूर्तिकला के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री हरे रंग की फ़िलाइट और ग्रे-नीली अभ्रक शिस्ट थी, जो सामान्य रूप से पहले के चरण से संबंधित थी और प्लास्टर, जिसका उपयोग तीसरी शताब्दी के बाद तेजी से किया गया था। मूर्तियों को मूल रूप से चित्रित और सोने का पानी चढ़ा हुआ था।
कुषाण कला: गांधार शैली और मथुरा शैली
गांधार कला का स्कूल कुषाण वंश के दौरान, विशेष रूप से सम्राट कनिष्क और उनके उत्तराधिकारियों के शासन के दौरान फला-फूला। इस प्रकार इसे कुषाण कला की एक शैली माना जाता है। कुषाण कला का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप लगभग उसी समय मथुरा (अब उत्तर प्रदेश, भारत) में विकसित हुआ।
गांधार और मथुरा कला के स्कूलों ने स्वतंत्र रूप से बुद्ध को चित्रित करने की अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। समय के साथ, दोनों स्कूलों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। सामान्य प्रवृत्ति एक प्राकृतिक अवधारणा से दूर और एक अधिक अमूर्त छवि की ओर थी।
गांधार शैली में केवल बौद्ध धर्म से सम्बंधित मूर्तियाँ बनायीं गयी जबकि मथुरा में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियाँ , जैन धर्म से सम्बंधित मूर्तियां शामिल है लेकिन मथुरा शैली में ज्यादातर मुर्तिया बोध धर्म से ही सम्बंधित रही।
यह आर्टिकल आधिकारिक स्त्रोत जैसे प्रमाणित पुस्तके, विशेषज्ञ नोट्स आदि से बनाया गया है। निश्चित रूप से यह सिविल सेवा परीक्षाओ और अन्य परीक्षाओ के लिए उपयोगी है।
Share and follow
अगर यह आर्टिकल आपको उपयोगी लगा तो इसे शेयर करना न भूले और नीचे दिए लिंक पर फॉलो भी करे